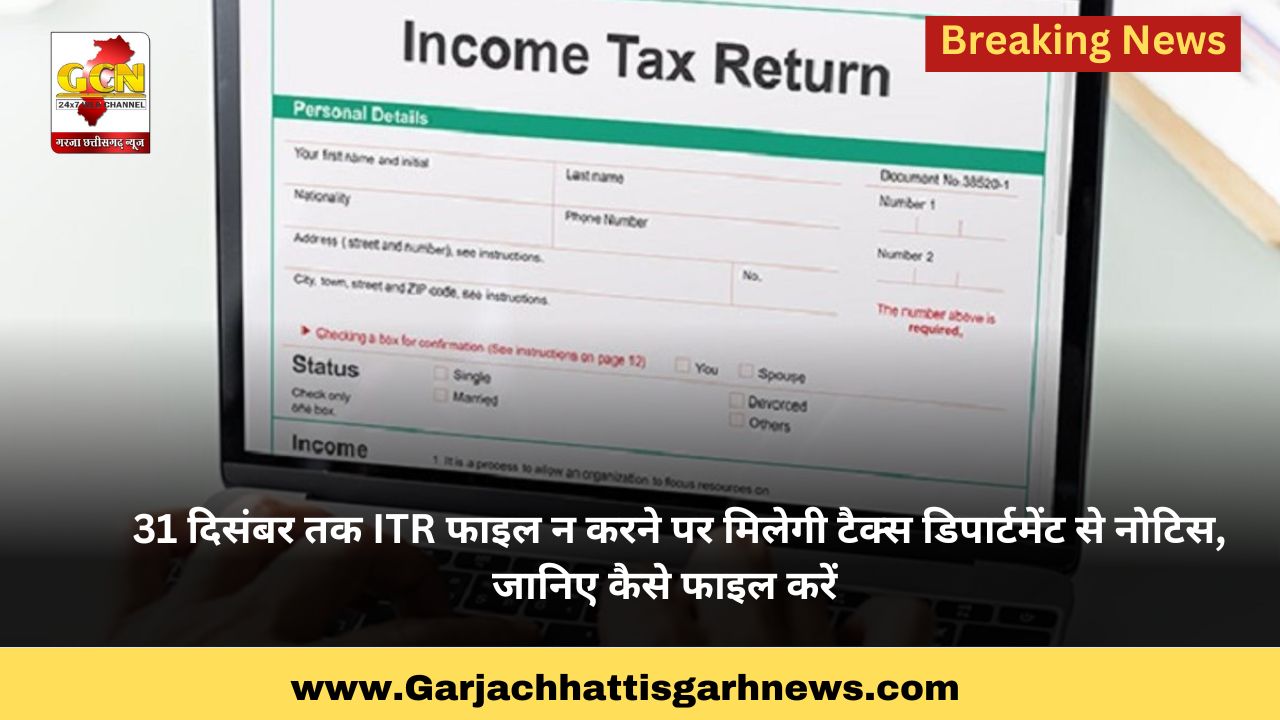बीजेपी के जिस दफ़्तर की दीवारें जहां कभी सिर्फ़ दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर हुआ करती थीं, आज वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी-बड़ी तस्वीरें आवेज़ां हैं। ऐसा क्यों है?क्या ये नज़रीयाती तब्दीली है या महज़ चुनावी मजबूरी? ब- ज़ाहिर ये एक कोशिश है जिसका हदफ़ बिहार की 2025 की असेंबली इंतेख़ाबात में दलित और पसमांदा वोट बैंक को अपनी तरफ़ माइल करना है।
गुज़िश्ता लोकसभा इंतेख़ाबात के नतीजों ने बीजेपी को वाज़ेह पैग़ाम दिया है कि सिर्फ़ आला जातियों पर इनहिसार अब कामयाबी की ज़मानत नहीं बिहार जैसी रियासत में जहां दलित, ओबीसी, एससी / एसटी और पसमांदा वोटरों की मुश्तरका तादाद 65 फ़ीसद से ज़ायद है, वहां सियासी जमाअतें अब अपनी हिकमत-ए-अमली तब्दील करने पर मजबूर हो रही हैं।
पसमांदा तबके की क़ियादत और उनके वोट को मुनज़्ज़म अंदाज़ में हासिल करने के लिए बीजेपी अब “सबका साथ, सबका विकास" के नारे के साथ-साथ "सबका विश्वास" जीतने की मुहिम भी चला रही है। हालाँकि ये सिर्फ़ नारे हैं, हक़ीक़त में बरसर - ए - इक्तिदार पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एतिमाद महज़ तस्वीरें लगाने और नारों से हासिल हो सकता है? या अमली तौर पर भी कुछ काम करने होंगे? और क्या जनता इतनी नासमझ है कि चंद दिनों के लिए तस्वीरें लटकाने से ही अपना क़ीमती वोट जाया कर देगी?
क़ाबिले- ज़िक्र है कि दो साल क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक जलसे के दौरान पसमांदा मुसलमानों का ज़िक्र करते हुए उनकी पसमांदगी पर हमदर्दी जताई थी। उनके बक़ौल, “पसमांदा मुसलमानों को माज़ी की हुकूमतों ने धोखा दिया है।" ये बयान सुनने में ख़ुशआइंद ज़रूर है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वाक़ई मर्कज़ी हुकूमत पसमांदा मुसलमानों की ख़ैरख़्वाह है तो फिर आइन-ए-हिंद का वो इमतियाज़ी ऑर्डर सदरती हुक्म 1950- • आज तक क्यों नाफ़िज़ -उल-अमल है ? जिसके तहत मुसलमान या ईसाई दलित आज भी रिज़र्वेशन से महरूम हैं। अगर वाक़ई नीयत साफ़ है तो इस इमतियाज़ी हुक्म को ख़त्म कर के पसमांदा मुसलमानों को भी वही हुकूक दिए जाएं जो दूसरे दलितों को हासिल हैं। सिर्फ़ जलसों में नाम लेना, इंतेख़ाबी मंशूर में ज़िक्र करना और तस्वीरों के ज़रिए हमदर्दी ज़ाहिर करना काफ़ी नहीं, हक़ीक़ी इंसाफ तो पॉलिसी और क़ानून में तब्दीलियों से मिलेगा ।
और 75 साल गुज़रने के बाद भी देश रत्न बख़्त मियां उर्फ बतख मियां अंसारी आज भी इंसाफ़ के मुन्तज़िर हैं। वो कौन सी हुकूमत होगी जो उन्हें इंसाफ़ दिलाएगी या फिर सिर्फ़ "पसमांदा, पसमांदा” का राग ही आलापना काफ़ी है? दूसरी तरफ़, ये भी एक तल्ख़ हक़ीक़त है कि आज कई ऐसी पसमांदा मुस्लिम तंज़ीमें मौजूद हैं जो दानिस्ता या ग़ैर-दानिस्ता तौर पर बीजेपी के नज़रीये को मज़बूत करने में मसरूफ़ हैं। चाहे वो कोई पसमांदा मोर्चा हो, पसमांदा सभा हो कोई भी हो। सवाल ये नहीं है कि वो बीजेपी के साथ क्यों खड़ी हैं, सवाल ये है कि क्या वो वाक़ई अपने तबके के मफ़ाद में कोई तबदीली ला पाई हैं? न तो 1950 का सदरती हुक्म ख़त्म हुआ, न रिज़र्वेशन मिला, न तालीमी या मआशी तरक़्क़ी के लिए कोई ख़ास स्कीम दी गई - फिर ये क़ुरबत किस बुनियाद पर है? यक़ीनन ये मोहब्बत तो नहीं हो सकती, शायद मज़बूरी है या फिर सियासी मसलेहत। लेकिन क्या मुसलमान सिर्फ़ इस्तेमाल किए जाने के लिए रह गए हैं? सब तबक़ात को हुक़ूक़ मिल रहे हैं, मगर मुसलमान अब भी इफ़्तिदार के दरवाज़े से बाहर खड़ा है। वक़्त आ गया है कि पसमांदा तंज़ीमें अपना मुहासा करें: क्या वो वाक़ई अपनी क़ौम के मफ़ाद की नुमाइंदा हैं या महज़ इक्तिदार के मातहत काम करने वाले ?
गौरतलब है कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने तमाम रियास्ती इलेक्शन ऑफ़िसरों को हिदायत दी है कि वोटर लिस्ट में फ़र्ज़ी तरीक़े से जुड़े हुए नामों, मरहूमीन के नाम, और दुहरे इंद्राज ख़त्म कि जाएं। ये हिदायत अगरचे जम्हूरियत के इस्तिहकाम के लिए ख़ुशआइंद है, मगर ख़द्शा है कि इसकी आड़ में मख़सूस समाजी तबक़ों के वोटरों को निशाना न बनाया जाए। बिहार में पहले भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि अक़ल्लीयतों और पसमांदा तबक़ात के वोट दानिस्ता तौर पर वोटर लिस्ट से हज़्फ़ किए जाते हैं। और उन्हें परेशान करने के लिए तमाम तरह के हर्बे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं।
ये बात भी क़ाबिले-गौर है कि बिहार की सियासत में दलितों, ओबीसी और पसमांदा वोटरों की हैसियत हमेशा फ़ैसला कुन रही है, मगर अफ़सोस कि उनकी सियासी हैसियत को अक्सर महज़ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पार्टियाँ उनको क़ियादत में हिस्सा नहीं देतीं, सिर्फ़ उनके चेहरों को दिखा कर वोट हासिल करने की कोशिश करती हैं। नतीजा ये होता है कि जब हुकूमत बनती है तो पॉलिसी साज़ी में अक़ल्लीयत और पसमांदा तबकात नदारद रहते हैं या यूं कहें कि उन्हें इससे महरूम रखा जाता है।
बिहार में शेख, सैयद, पठान जैसी आला जात मुस्लिम तबक़ों के बरअक्स, अंसारी, क़ुरैशी, सलमानी, धोबी, हलवाई, मोमिन, मंसूरी जैसे पसमांदा मुसलमानों की अक्सरीयत तालीम, मआशत और सियासत में पिछड़ चुकी है। उनके लिए 1950 का सदरती हुक्मनामा आज भी सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, जिसके तहत मुसलमान और ईसाई दलितों को रिज़र्वेशन से महरूम रखा गया। यही वो तबका है जो तालीम, सेहत, रोज़गार और इंसाफ़ के लिए सबसे ज़्यादा रियासत पर इनहिसार करता है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी असेंबली से लेकर पंचायत तक में न के बराबर है।
बिहार के दलित, एससी / एसटी, ओबीसी और पसमांदा मुसलमान अब वो पुराने वोटर नहीं रहे जो नारों से बहल जाएं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे वोट से हुकूमत बनती है, मगर हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिलती? हमें हर पाँच साल बाद याद किया जाता है, लेकिन पाँच साल तक भुला क्यों दिया जाता है? हमारे नाम पर पॉलिसियाँ बनती हैं, लेकिन फ़ायदा ऊँचे तबक़ों को क्यों पहुँचता है? ये सवाल अब सिर्फ़ जलसों में नहीं बल्कि चारों तरफ़ चौक-चौराहों पर भी गूंज रहे हैं।
ये भी हक़ीक़त है कि पसमांदा मुसलमानों का मामला और भी ज़्यादा पेचीदा है। उनके मसाइल, जैसे तालीम, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़, रिज़र्वेशन और समाजी इंसाफ़ वग़ैरा क़ौमी और रियास्ती सियासी मंज़रनामे से ग़ायब हैं। चंद पसमांदा रहनुमाओं जैसे अब्दुल कय्यूम अंसारी, अली हुसैन आसिम बिहारी वग़ैरा को आगे लाकर पसमांदा तबक़ात के जज़्बात को बहलाया जाता है। इसकी ज़िम्मेदार सब ही पार्टियाँ हैं चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू या कोई और सियासी पार्टी - सब ने मिल कर पसमांदा समाज का इस्तेहसाल किया है और उनके हुक़ूफ़ के लिए ज़मीनी सतह पर मेहनत नहीं की और न ही उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए कोई ठोस इक़दामात किए और उनके तालीमी और इक्तिसादी हालात सबके सामने हैं।
दिलचस्प बात ये है कि जिन तंज़ीमों ने कभी अंबेडकर के ख़यालात को "समाज को तोड़ने वाला” कहा था, आज वही उन्हें "राष्ट्र नायक" क़रार दे रही हैं। ये तज़ाद इस बात का सुबूत है कि नज़रिया कभी -कभी सिर्फ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, असल मक्सद इक्तिदार का हुसूल होता है।
आने वाले बिहार असेंबली इंतेख़ाबात में असल सवाल यही होगा कि दलित, ओबीसी और पसमांदा मुसलमान क्या अपने मसाइल के हल की बुनियाद पर वोट देंगे? क्या वो महज़ तस्वीरों, वादों और ज़ात-पात की सियासत से ऊपर उठ कर अपनी हक़ीक़ी क़ियादत को पहचानेंगे और अपनी ख़ुद की क़ियादत खड़ी करेंगे?
अगर सियासी जमाअतें वाक़ई दलितों और पसमांदा तबक़ात की तरक़्क़ी की ख़्वाहां हैं, तो उन्हें सिर्फ़ पोस्टर पर तस्वीर लगा कर या किसी दलित को रियास्ती सदर बना कर ख़ुशफ़हमी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि ज़मीन पर इस्लाहात, तालीम, तहफ्फुज़, रोज़गार, रिज़र्वेशन और इंसाफ़ के हक़ीक़ी इक़दामात करने होंगे।
ये वक़्त है जागने का, पहचानने का, और सिर्फ़ "नज़रीयाती तस्वीरों" पर न बहकने का। सियासत को अगर बदलना है, तो वोटरों को भी अपना मिज़ाज बदलना होगा। अब की बार "सियासत में हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं" का नारा पूरे बिहार में गूंजे तभी पसमांदा और पिछड़े तबक़ात अपना आइनी हक़ हासिल कर सकते हैं वरना आइंदा पाँच साल फिर ज़ुल्म-ओ-सितम, तशद्दुद और दूसरों के रहम-ओ-करम के लिए तैयार रहें - यही ज़मीनी हक़ीक़त है जिसे इस इंतेखाब में ज़रूर बदलना होगा ।



















.jpg)